जब मैंने पहली बार शराब को अपने हलक में उतारा था। अपने शरीर में मुझे एक अजीब सी झनझनाहट महसूस हुई थी, वैसे ही जैसे किसी अनजान वीराने में हवा का अजनबी झोंका भी हमारी रूह को बेचैन कर देता है। मधुशाला पढ़ने से पहले ही मैं दोस्तों की देखा-देखी मधुशाला का दीदार करने गया था। मधु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। बहुत कुछ सुनना अभी भी बाक़ी है। मदिरा की पहली घूँट छाती को तेज़ाब-सी जलाते हुए उदर तक पहुँचती है। मदिरा जब हाला बनकर दिमाग़ पर चढ़ती है, तब जाकर कहीं साक़ी का दीदार होता है। मुझे अपनी “पीड़ा में आनंद” यहीं तो नसीब हुआ है। यही तो मेरी मधुशाला है, आपकी तरह ही मैं भी अपना इहलोक ही तो रचता हूँ। यहीं तो पहली बार मैं ख़ुद के लिए एक अच्छी सी आत्म-अवधारणा को रच पाया हूँ। अपने इहलोक को मुकम्मल बनाने की ज़िम्मेदारी ही तो हमारी है। पर, अपने इहलोक में हम अकेले नहीं होते हैं। कोई ना कोई चेतना हमें निहार ही रही होती है।
मेरे इहलोक ने जाने-अनजाने मुझे कई बार बेवजह ही दुत्कार भी है। कई बार बिना किसी कारण ही दुलारा भी है। ना जाने उसने मुझमें ऐसा क्या दिखता आया है? पर, मेरे इहलोक की मधुशाला में मदिरालय भी है। जहां बैठने की कोई वजह मेरे किसी चाहने-वाले के पास तार्किक तो नहीं ही थी। इसलिए, बेवजह कोई वहाँ मुझे परेशान नहीं करता था। वहाँ परेशान होने की सबकी अपनी-अपनी वजह तो थी। वहाँ दुतकारने की भी वजह है, साथ ही लापरवाह मज़ाक़-मस्ती भी है। नशे में किसी ने मेरा अपमान किया हो, ऐसा मुझे तो याद नहीं है। अपने दोस्तों की स्मृति पर भी मुझे पूरा भरोसा है।
मदिरालय में बैठकर हम परीक्षाओं की तैयारी नहीं करते थे। लोकतंत्र की इन परीक्षाओं से ऊबकर ही तो हम सब वहाँ पहुँचे थे। जब अपने ज्ञान पर हमें ख़ुद ही भरोसा नहीं था, तो ज्ञान का भ्रम ही पालने में क्या बुराई थी?
हम सपनों में भी संशय और तर्क रचते जाते थे। ना जाने हमने कितने बहाने बनाये थे? हर बहाने हमने साहित्य से ही कहाँ चुराये थे। कुछ बहाने हमने अपने भी तो बनाये थे। वहाँ भी तो साहित्य निखर ही रहा था। अफ़सोस! वहाँ कोई ईमानदार पाठक नहीं था। नशे में मदहोश मैं या मेरे किसी दोस्तों ने गलती से भी ज्ञान की कोई बात नहीं की होगी। क्योंकि, ऐसा करना हमें कभी ज़रूरी ही नहीं लगा। इस लोकतंत्र को ही ज्ञान की ज़रूरत कहाँ है?
ज्ञान की बात तो बस शिक्षक, शिक्षा और वैसे होनहार छात्र करते हैं, जो इस शिक्षा-व्यस्था के पंडित माने जाते हैं। बाक़ी कोई करे तो लोकतंत्र उसे बकवास मानता है। औपचारिक शिक्षा के बहाने सफलता के प्रमाण-पत्र बाँटे जा रहे हैं। उसमें भी यह लोकतंत्र हर किसी को संतोषजनक प्रमाण-पत्र देने में भी असमर्थ है। मैं उस बहुमत का हिस्सा हूँ, जिसकी परवाह इस लोकतंत्र को कभी थी ही नहीं। मैं भी अकेला कहाँ हूँ?
मेरा पूरा इहलोक ही मेरा प्रत्यक्ष है। वह ख़ुद को पाठशाला में अकेला पता है। तभी तो यारी निभाने जवानी मधुशाला जा पहुँचती है। मधुशाला से मेरे याराना का दायरा मेरी यात्रा और मंज़िल के अनुसार बनता-बिगड़ता आया है। उधार ही सही, जब भी मैंने होनहार छात्र का मुखौटा पहना है, इसी लोकतंत्र ने भी मेरी सुंदरता को सराहा है। मुखौटे के उतर जाते ही मेरा असली चेहरा देखकर मेरा इहलोक भी भयभीत हो उठता है। लगता है, जैसे मेरे इहलोक को भूल जाने की बीमारी है। वह अपना ही कड़वा सच भुला जाती है। दुबारा जब कभी गलती से मुलाक़ात होती है, तो सच को कड़वा बताती है। मीठी तो ज़ुबान होनी चाहिए, कड़वी तो शराब भी होती है।
लोकतंत्र दवा में भी दारू मिलकर बेच रहा है। दवा की दुकानों से जितनी मदिरा मेरा इहलोक अपने-अपने घर लाता है, उतनी कभी किसी मैखानों में भी कहाँ बिकी होगी। पर दवा की ज़रूरत वह जानता है, क्योंकि लोकतंत्र ने ही उसे बतायी है। अपनी मधुशाला की ज़रूरत समझने के लिए ही तो आत्मनिर्भर होना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर अपनी ज़रूरतों को हम समझ पाते, तो शायद अपने बच्चों की औक़ात को तंत्र के दिये प्रमाणपत्रों के आधार पर नहीं आंकते।
पर, मेरा इहलोक तो उन्हीं छात्रों को होनहार बताता है, जो अपनी अभिव्यक्ति लोकतन्र के प्रमाण-पत्रों पर ही कर पाते हैं। बस, अपने दिये प्रमाणों पर लोकतंत्र को भरोसा है। मेरा इहलोक भी वही प्रमाण मुझसे भी माँगता है। हर पंडिताई हर बच्चे की समझ नहीं आती है। सच ही है, कुछ बच्चे ही अछूत पैदा हो जाते हैं। जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जीवन की नसों में शिक्षा का ज़हर भर रही हैं।
मैंने कई बार अपने शिक्षकों से पूछा - “कोई लेखक कैसे बनता है? कैसे कोई कलाकार बन जाता है? कोई नेता ही कैसे बन पाता है? प्रधानमंत्री बनने की पढ़ाई किस कॉलेज में होती है?”
पर, जहां लोक-सेवक बनने-बनाने का धंधा ज़ोर-शोर से चालू है, वहाँ मेरे इन बुनियादी या बेबुनियादी सवालों का जवाब भला किसे देने की फ़ुरसत थी?
आजतक, किसी बुद्धिजीवी ने मुझे शिक्षा की ज़रूरत का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। उनका हर तर्क औपचारिक शिक्षा की ज़रूरत तक ही सीमित रह जाता है। लेखकों के प्रति उनकी अवधारणा अक्सर दरिद्रता से ही ग्रस्त रहती है। सफलता के कुछ ही उदाहरण हमें ऐसे मिलते हैं, जब लेखक अपनी रचना का उचित अर्थ अपने इहलोक से निकाल पाता है। कला और साहित्य में सफलता की गारंटी देने से तंत्र साफ़ इनकार कर देता है। रचने का कोई वैज्ञानिक फार्मूला अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रयास चालू है, कुछ सफलताएँ में लोक ने पायी हैं। कृत्रिम बुद्धि भी अपने आप में एक अद्वितीय कलाकारी है।
आख़िरकार, एक रचियता तो ख़ुद में बसे ब्रह्म को ही अभिव्यक्त कर पाता है। रचना तो हर क्षेत्र में संभव है। विज्ञान भी तो रचता है। पर, एक बार रचकर वह रचने की ज़िम्मेदारी को तकनीक के हवाले कर देता है। पहली कार या पहला कंप्यूटर या कोई भी अन्य उत्पाद जो बाज़ार हमें बेच रहा है, पहली बार किसी कारख़ाने में नहीं बना था। पहले, किसी रचियता ने फ़ुरसत से उसे पहली अपनी कल्पनाओं में सजाया था। फिर, कर्म-इंद्रियों और वस्तुओं की मदद से उसे वह मूर्त रूप देता है। उस मूर्त में जान फूंक देना क्या किसी चमत्कार से कम है?
पहुँचते-पहुँचते इंसान चाँद तक पहुँचकर, उससे भी कहीं आगे निकल गया। पृथ्वी गोल है, या चौकोर — आज इस पर लोकतंत्र बहस नहीं करता है। यह सामान्य ज्ञान का हिस्सा है। पर, वही सामान्य ज्ञान हमें यह भी तो बताता है कि रामायण की रचना किसने की थी? हमारे पास पुख़्ता प्रमाण हैं कि धरती गोल ही है। सपाट धरती का संशय और जगत के केंद्र में पृथ्वी के होने का भ्रम अब हमारी चेतना से कोसों दूर हो चुका है। इसलिए, लोकतंत्र को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अपेक्षा करता है कि ऐसे तथ्य छात्रों और नागरिकों को कंठस्थ होने चाहिए। पर, कला के ज्ञान में विज्ञान के प्रमाणों की दरकार कहाँ होती है?
विज्ञान की जननी भी कला ही है। भाषा नहीं होती, साहित्य नहीं होता, तो विचार ही कहाँ होते? बिना विचारों के विज्ञान भला क्या करता? इसलिए, जहां-जहां कल्पना होगी, कला का वहाँ होना अनिवार्य है। कला की परिभाषा भी तो काल्पनिक ही है। गूगल महाराज से जब मैंने पूछा, तो कला की ऐसी ही एक परिभाषा तक उसने मुझे पहुँचाया — “कला हमारे मन की कल्पनाओ को प्रकट करने का एक माध्यम है जिसे हम अपनी इच्छानुसार भिन्न-भिन्न स्वरूप देते है, अर्थात कला को मानवीय भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति कहा गया है।”
क्या बिना कल्पनाओं के विज्ञान संभव है?
शायद! होगा! इस व्यावहारिक जगत में, मेरा इहलोक सूचना-क्रांति कर चुका है। मेरे स्कूल का होमवर्क अब मेरा स्मार्टफ़ोन करने के काबिल हो चुका है। यहाँ तक कि अब वह अपने दम पर छोटे-मोटे निबंध और कवितायें लिखने में भी समर्थ है। यही नहीं थोड़ी-बहुत चित्रकारी भी अब वह बिना कलम-कूँची उठाये करने में भी सक्षम है। इस लोकतंत्र की कई कलाकारी से मेरा परिचय तो मेरा आईफ़ोन ही करवाता है। इस मिथक जगत में हमने अपनी सुविधा के अनुरूप एक आभासी दुनिया भी बसा रखी है। ये शब्द भी जो मैं अभी लिख रहा हूँ, वे भी आभासी ही तो हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद — जब, मैंने दर्शनशास्त्र की औपचारिक परीक्षा में अपनी क़िस्मत आज़माई, तब जाकर मेरी बेरोज़गारी दूर हुई। जीविकोपार्जन की समस्या अभी भी मेरे अस्तित्व पर मंडराती है, पर अर्थोपार्जन की दरिद्रता का बोध अब मुझे कम ही होता है।
दर्शनशास्त्र के अंतर्गत नीतिशास्त्र की भी पढ़ाई होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि न्याय और नैतिकता के निर्धारण हेतु सिर्फ़ कार्य ही नहीं, कारण भी ज़रूरी होता है। सिर्फ़ हिंसा ही नहीं, उसकी मंशा भी कार्य की नैतिकता का निर्धारण करती हैं। वरना, एक जैसी हिंसा का ही तो लोकतंत्र शिकार है। अपने कल-कारख़ानों में पहले तंत्र हथियार बनता है। फिर लोक को थमता है। साथ ही उसके उपयोग की नैतिक ज़िम्मेदारी वह लोक पर छोड़ देता है। प्रयोग के अनुसार फिर लोकतंत्र किसी को आतंकवादी घोषित कर देता है, और किसी को सैनिक बना देता है। बस, ऐसे ही लोकतंत्र का व्यापार चलता जाता है। अरे! हथियार बनाना ही ज़रूरी क्यों था? ना होते हथियार, ना किसी की हत्या होती!
पर, इस असुरक्षित लोकतंत्र में हमें ना जाने किन-किन ख़तरों से निपटने के लिए हथियार बनाने पड़े?
जिसने पहले ज़हर की खोज की होगी, उसने किसी की हत्या का षड्यंत्र रचाया होगा, ज़रूरी तो नहीं है। ज़हर का इलाज ही जब ज़हर से संभव है, तो कोई भला साँप को बिना मारे ज़हर भी कहाँ से लाएगा?
साँप का गला घोंटकर उसका ज़हर निकाल पाने का पौरुष कहाँ देखने को मिलता है?
इसलिए, बिना हथियार के इस सभ्यता की कल्पना भी बेईमानी है। जब, ज़हर भी ज़रूरी है और जहां, हथियार भी अनिवार्य हैं, वहाँ नैतिक समस्याओं की उठा-पटक तो चलती ही रहेगी। पर, यहाँ हम सामाजिक और व्यावहारिक नैतिकता के निर्धारण का प्रयास कर रहे होते हैं। क्या नैतिकता काल्पनिक भी हो सकती है?
दर्शनशास्त्र के अपने सीमित अध्ययन के आधार पर मुझे तो पारिभाषिक स्तर पर ऐसी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। नीतिशास्त्र भी व्यवहार के रास्ते विचारों तक ही नैतिकता की बातें करता है। पर, मेरे इहलोक ने तो अपनी कल्पनाओं पर ही नैतिकता का बोझ उठाये रखा है। ना जाने, किन किरदारों की अस्मिता का मिसाल लोकतंत्र हमें आये दिन देता रहता है, जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तक मौजूद नहीं है? नैतिकता का निर्धारण करना साहित्य का काम नहीं है। दर्शन ने साहित्य को कभी यह छूट नहीं दी है। रचियताओं ने भी शायद ही कभी ऐसा भ्रष्टाचार किया होगा। यह तो लोकतंत्र के चंद व्यापारी हैं, जो शिक्षा के नाम पर हमारे सपनों का धंधा कर रहे हैं।
विचार और कल्पना में अंतर होता है। विचारों को प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विचार से व्यवहार प्रभावित होते हैं। व्यवहार अपने आप में स्वतः प्रामाण्य है। हम जहां भी होते हैं, अपने व्यवहार का प्रमाण लिए खड़े होते हैं। यही तो हमारा सच है, जिसे हम बदल देना चाहते हैं। पर, हमारी कल्पनाओं पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। कल्पनाओं से तो बस हमारे कुछ ही विचार प्रभावित हो पाते हैं, जो शायद ही कभी हमारे व्यवहार का कारण बन पाने के काबिल हो पायें। विचारों की अभिव्यक्ति भाषा से संभव है। पर, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यह अनंत ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाता है। विचारों की ज़रूरत लोकतंत्र को पड़ती है, पर हमारे इहलोक की रेलगाड़ी तो कल्पनाओं की पटरी पर चल सकती है। इसलिए, बस विचार ही ज़रूरी नहीं हैं। कल्पनाएँ भी ज़रूरी हैं। पर कल्पनाओं पर नैतिकता का पहरा लगा देना किसी भी लोकतंत्र के लिए कहाँ से नैतिक है? विचारों और कल्पनाओं की इसी नैतिक रंजिश ने मेरे इहलोक का बंटाधार कर रखा है।
ना जाने कितनी वैकल्पिक और मायावी कल्पनाओं का रिश्ता-नाता लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है?
ना जाने मेरे इहलोक ने कैसे-कैसे भ्रम पाल रखे हैं?
देखिए! गौर से देखिए! तभी शायद सच को हम झूठ से छल पायेंगे। मधुशाला की बेहया लालसा ही तो मुसाफ़िरों में सपने भरती आयी है। सुख की आशा ही यात्रा पर बने रहने की प्रेरणा यात्रियों को देती आयी हेल।
जब तक कल्पनाओं को ही हम विचारों से अलग नहीं कर पायेंगे, हम सच को कहाँ तलाश पायेंगे?
हर कल्पना विचार नहीं होती है। पर, विचारों का काल्पनिक होना तो निर्धारित है। किसी सच या तथ्य का विवरण ही तो है। हर विचार भी हमारी अवधारणा का हिस्सा बन ही जाये, यह भी कहीं से ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति, परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार हमारे फ़ैसले बदल सकते हैं। एक फ़ैसला बदल जाने से पूरी कहानी ही बदल जाती है। साला! बस एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है।
ज़रूरतों से इच्छाओं का जन्म होता है। इच्छाओं से हमारी मनोकामना जुड़ जाती है। मनोकामना से महत्वाकांक्षा तक का सफ़र मेरे इहलोक ने पहले ही मेरे लिए भी तय कर रखा था। तभी तो मैं अपने इहलोक से नाराज़ भी हूँ, ग़ुस्सा भी। यह मेरी अवधारणा है, जो मेरे व्यवहार को विद्रोही बन जाने को मजबूर कर देता है। विचार भी अक्सर हमारी रचना को ही प्रभावित कर पाते हैं। हमारे व्यवहार का निर्धारण मुख्यतः हमारी अवधारणाएँ करती हैं। क्योंकि हर फ़ैसले पर हम वैचारिक मंथन के बाद ही नहीं पहुँचते हैं। हमारी कुछ प्रतिक्रियाओं को भी लोकतंत्र हमारा व्यवहार मान लेता है। क्या बस मान लेने से ही ज्ञान हासिल हो जाता है? क्या प्रयाप्त प्रमाण के बिना किसी सूचना को अपनी अवधारणा में शामिल कर लेना बुद्धिमानी है? क्या यही प्रज्ञा है? क्या यही धर्म है? क्या हमारी ज़रूरतों का नैतिक या धार्मिक होना ज़रूरी है?
हमारी हर ज़रूरत भौतिक नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति और प्राणी की ज़रूरतें पूर्व-निर्धारित नहीं हो सकती है। कृषि-सभ्यता के विकास में बारिश की अहम भूमिका थी। जिसकी भविष्यवाणी आज एक हद तक संभव भी है। पर, त्रेता युग में जब राम-राज्य था, तब मौसम वैज्ञानिक नहीं थे। शायद इसलिए, बारिश के लिये होम-हवन का रीति-रिवाज शुरू हुआ होगा। होम-हवन से कुछ हो ना हो, एक साथ बैठकर भजन-कीर्तन करने से समय तो अच्छा गुजर ही जाता है। फिर कब मेघ घिर आते हैं? कब वे बिजुरी की तलवार के साथ बूँदों के बान बरसने लगते हैं? किसी को पता ही नहीं चलता होगा। सबको भ्रम हो गया कि होम-हवन करवाने से ही बारिश हुई होगी। पर भरोसा एक बार में नहीं होता है। आस्था के लिये सिर्फ़ चमत्कार ही काफ़ी नहीं है। जिन चमत्कारों का रहस्य हम जान जाते हैं, वे ही तो जादू कहलाते हैं। चमत्कार से श्रद्धा की भावनात्मक ज़रूरत पूरी हो सकती है। पर, आस्था को जादू की दरकार होती है। जादू वही होते हैं, जिनका प्रमाण जादूगर के पास होता है। चमत्कार कैसे होता है? कौन जानता है?
जो जान जाता है, वही रचियता बन जाता है। कुछ चमत्कार ऐसे भी होते हैं, जिन्हें हमारी आखें देख नहीं पाती है। पर, हमारी चेतना को वे मोह-माया के बंधन में जकड़े रखते हैं। उनका जादू मन पर जो होता है। जादूगर के जादू को तो हम सब ने देख है। चमत्कार के विज्ञान को ही तो जादू कहते हैं। पर, जादूगर कितना भी मायावी क्यों ना हो? बिना अपना आवरण उतारे और अपनी कला का प्रमाण दिये, वह पूज्य कभी नहीं बन पाता है। क्योंकि, उसके प्रति लोक की अवधारणा ही यही है कि वह छल से उन्हें भ्रमित कर अपना जादू दिखलाता है। कोई जादूगर अगर अपने जादू को कला के रूप में पेश करता है, तो समाज भी उसे स्वीकार करता है। मैंने भी ना जाने कितने जादूगरों के शो के टिकट ख़रीदे हैं। आज भी ख़रीदता हूँ। पर, इस स्मार्ट जमाने में हर कोई ख़ुद को जादूगर ही समझता है। झट से यूट्यूब खुला, पट से जादू की छड़ी घुमाना आ गया। सच को जानकर ही लोक एक नैतिक अवधारणा बना पता है। तब तक अवधारणाएँ लोक के भ्रम पर ही टिकी होती है। हमारी अवधारणाएँ तो नित्य-प्रतिदिन बनती बिगड़ती रहती हैं। हर नयी सूचना हमारी अवधारणाओं के साथ छेड़खानी करने में सक्षम हैं। अब यह तो हमारी आस्था और प्रज्ञा पर निर्भर करता है कि किन सूचनाओं को हम तरजीह देंगे, और किसे नहीं?
त्रेता युग के तांत्रिकों को लोकतंत्र ने बहुत हद तक तड़ीपार कर दिया है। पर, अपने ही भ्रम और संशय का शिकार मेरा इहलोक आज भी त्रेता युग के कई कर्मकांडों को निभा भी रहा है। आज भी होम-हवन चालू हैं। उस युग में बड़ी चालाकी से तांत्रिकों ने तत्परता से तब तक तपस्या की, जब तक बारिश नहीं हो गई। होम-हवन तब तक चलते रहे, जब तक सूखे खेतों में हरियाली नहीं छा गई। उनकी तपस्या भी तब व्यर्थ कहाँ थी? वैसे, इतना बेवक़ूफ़ तो मेरा इहलोक भी नहीं है। जबसे, मौसम वैज्ञानिकों ने लोकतंत्र में अपनी जगह बनायी है। तबसे, बेचारे देवताओं के राजा इंद्रदेव भी अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाने में ख़ुद को असफल पाते हैं। भला बिना किसी कांड के अब वे बहुत में कैसे आ पायेंगे? मैंने तो अपने इहलोक में इंद्रदेव का एक भी कार्यालय नहीं देखा है। पर, मेरे इहलोक का हर भ्रम अभी कहाँ टूटा है?
मेरा ही सपना कभी कहाँ पूरा हा पाया है? ना जाने कितने भ्रमों और संशयों से मैं ख़ुद अपनी चेतना को जूझते पाता हूँ। मैंने भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार इसी लोकतंत्र ने कई कल्पनाएँ उधार ले रखी हैं। इस कर्ज का सूद ही मेरा इहलोक नहीं जुटा पाता है, मूल वह कैसे चुकाएगा?
मेरे इहलोक में मिस्टर इंडिया भी मौजूद हैं, जो ग़ायब होना जानते हैं। मिस्टर इंडिया के चक्कर में मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ अदृश्य होने के विज्ञान पर कल्पना करने की कोशिश की। एक तो बड़ी प्यारी कल्पना भी थी, आईनों के टुकड़ों को हम अपने शरीर पर चिपका लेंगे। जब कोई हमें देखेगा, उसे वह ख़ुद नज़र आ जाएगा। हम किसी को कहीं नज़र ही नहीं आयेंगे। व्यावहारिक ना सही, पर यह भी संभव तो है। मेरे इहलोक में शक्तिमान भी है, जो किसी ड्रिल मशीन की तरह गोल-गोल घूमता हेलीकॉप्टर जैसा उड़ना जानता है। अजीब सी “फक-फक” की आवाज़ आती थी, जब शक्तिमान दूरदर्शन पर उड़ता था। त्रेता युग में पैदा हुआ होता, तो आज उसका भी कहीं एक मंदिर होता। क्या पता आज से सौ साल बाद पुरातत्व-विभाग को शक्तिमान मिल जाये, जो आज ही मेरे इहलोक से लगभग नदारद हो चुका है, तब सच में कोई उसका मंदिर बनवा डाले। बचपन से लेकर जवानी तक ना जाने साहित्य ने मुझे कितने इहलोक के भ्रमण का अवसर प्रदान किया है? इसमें टॉम-सॉयर भी है, तो हैरी-पॉटर भी है। शक्तिमान है, तो स्पाईडरमैन भी। रहीम भी हैं, तो राम भी। बस मेरे राम, रहीम, स्पाईडरमैन, शक्तिमान, हैरी-पॉटर, टॉम-सॉयर आदि वैसे ही नहीं हैं, जैसा लोकतंत्र मुझे ज़बरदस्ती दूरदर्शन पर दिखलाता है। यह अलग बात है कि मेरी कल्पनाओं का हैरी-पॉटर भी बिलकुल डैनियल जैकब रैडक्लिफ से मिलता है, जिसने हैरी-पॉटर का किरदार सुनहरे पर्दे पर निभाया है। मेरे जीवन में इंटरनेट के आ जाने के बाद, मैंने दूरदर्शन देखना लगभग बंद ही कर दिया है। दूरदर्शन पर दर्शन की स्वतंत्रता ही कहाँ थी?
आज तो स्मार्ट टीवी का जमाना है। फिर भी जाने-अनजाने कभी नुक्कड़ों पर, तो कभी गाँव-घर में दूरदर्शन का यह ड्रामा मुझे दिख भी ही जाता है। जैसे, अभी-अभी मोबाइल पर मैंने ऐसा कुछ देखा —
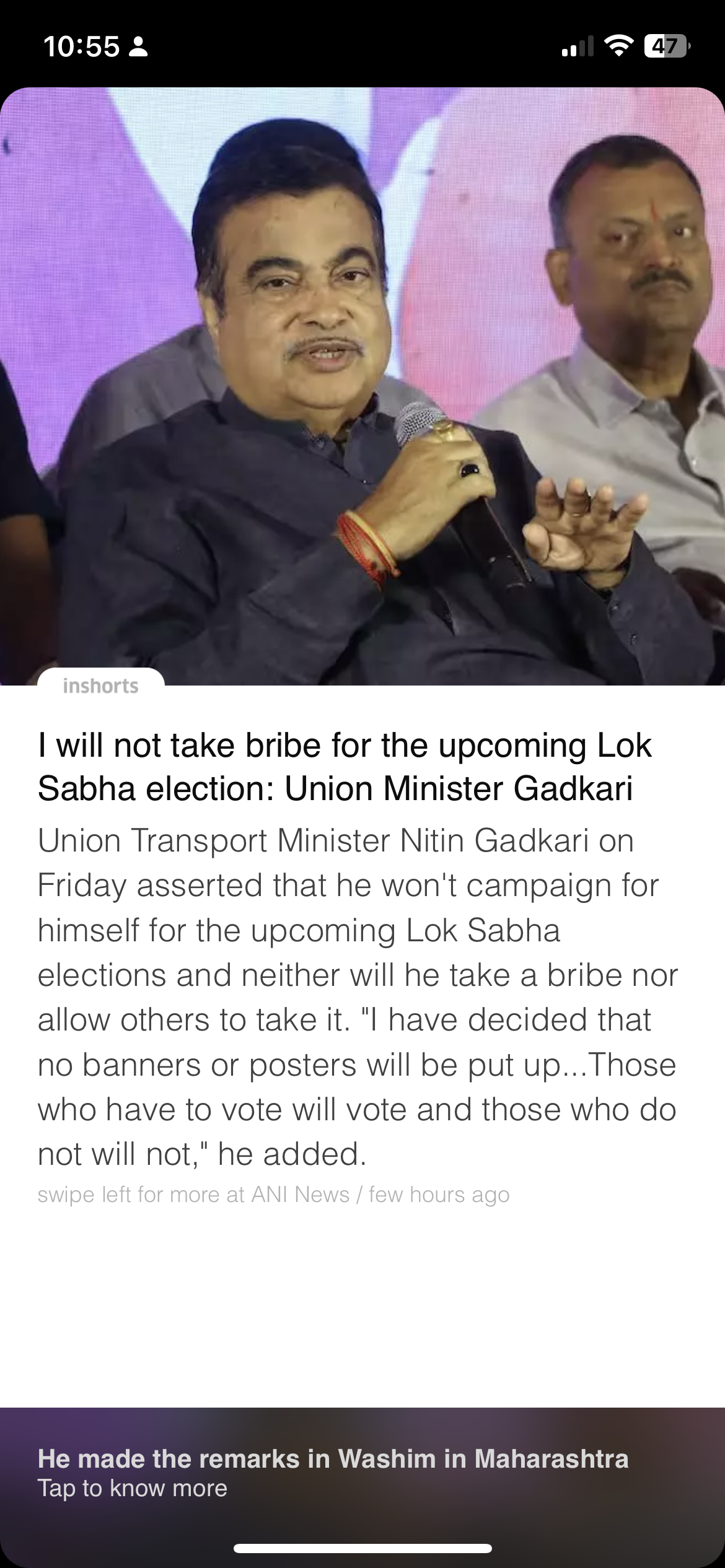
माननीय केंद्रीय मंत्री आगामी लोकतंत्र के चुनाव में लोक से यह वादा कर रहे हैं कि इस बार वे लोकसभा चुनाव में रिश्वत नहीं लेंगे। अब पता नहीं! मेरा इहलोक इतना भी अनुमान लगा पाएगा या नहीं कि महोदय, साफ़-साफ़ ख़ुद से यह कह रहे हैं कि पिछले लोकसभा के चुनावों में उन्होंने रिश्वत ली थी। तभी तो इस बार वे अपनी ईमानदारी का प्रमाण देने के लिए ख़ुद पर आरोप मढ़कर, भविष्य में अच्छे-दिनों का सपना दिखा रहे हैं। ऐसी विपदा में भी लोकतंत्र की कोई जैविक या वैकल्पिक कल्पना तक मेरे इहलोक से नदारद है। क्या यही लोकतंत्र है?
अपनी कल्पनाओं में मैं निरंकुश तानाशाह हो तो सकता ही हूँ। ऐसा करने से कोई कैसे मुझे रोक सकता है? शायद आप भी मुझे ऐसा ना करने की सलाह देते। मैं आपका आभारी भी होता। पर फिर मैं यह कल्पना भी कैसे कर पाता? जिसे आप अभी पढ़ रहे हैं। वैसे भी, मेरी कल्पनाओं से मेरे इहलोक को तो कोई अंतर नहीं पड़ जाएगा। फिर भी मैं जब अपनी ही कल्पनाओं को सत्य, सच या सही मान बैठता हूँ। तब, तानाशाही मेरी कल्पनाओं से ऊपर उठाकर मेरे विचारों का हिस्सा बन जाती है। जिससे मेरा व्यवहार प्रभावित होने लगता है। क्योंकि, मेरी अवधारणाएँ बदलने लगती है। मेरे व्यवहार को अगर बदलना है, तो मेरी अवधारणाओं को बदलना पड़ेगा। अनैतिक आचरण का लांछन लगाकर किसी का क्या भला हो जाएगा? अगर मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो! मैं किसी को भी यह कहाँ समझा पाता हूँ कि मैं तो सिर्फ़ अपनी कल्पनाओं में ही तानाशाह था? वे भी मेरी ही कल्पनाओं का शिकार हो, ख़ुद तानाशाह बन जाते हैं। ना जाने, मेरी इस रचना के लिए कौन-कैन सी सजा मेरे इहलोक ने सोच रखा होगा?
कल्पनाओं के विचार तक का सफ़र भरोसे के रास्ते तय होता है। पर, विचार के व्यवहार तक के रूपांतरण के लिए आस्था की ज़रूरत पड़ जाती है। आस्था हमारी अवधारणाओं पर निर्भर करती हैं। आस्था की मनोदशा के साथ उम्मीद की भावना जुड़ी होती है, जो कालांतर से हमें जीवन का राग सुनाती आयी है। इसी राग को कोई अपने भजन में दुहराता है, तो कोई अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करता है। मैं अगर इसे गालियों में अभिव्यक्त करना चाहता हूँ, तो किसी को क्यों आपत्ति है?
इस लोकतंत्र से जब भी मैंने पूछा — “अच्छा बताओ! कोई साहित्यकार कैसे बन जाता है?”
लोक प्रायः ख़ामोश ही रह गया। लँगड़ाता हुआ एक सुझाव तंत्र देता है कि जाकर किसी अच्छे स्कूल-कॉलेज में साहित्य पढ़ो। शायद, बुद्धि खुल जाये। पर, साहित्य पढ़ते हर बच्चे को तंत्र के विभिन्न फॉर्म भरते ही मैंने देखा है। मेरे पिताजी हिन्दी साहित्य के विभागाध्यक्ष हैं। वे भी मुझे और अपनी बहू को नये-ताजे निकले फॉर्म को भरने का ज्ञान देते ही रहते हैं। वैसे, लेखक बनने के लिए मुझे प्रोत्साहित भी उन्होंने ही किया है। वे भी तो लोकतंत्र की इस दरिद्रता और जीविकोपार्जन की ज़रूरत को जानते-समझते हैं। इसलिए, एक अदद नौकरी का आवेदन भरने के लिए भी हमें फुसलाते ही रहते हैं। हर माँ-बाप यही तो कर रहा है। मेरे माता-पिता ने भी अपनी हर ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई है। मैं बस अपनी ज़िम्मेदारी अपने अन्दाज़ में उठाना चाहता हूँ। पर, उन्हें मेरी बहुत फ़िक्र है। वे मुझे रोकना भी नहीं चाहते हैं, उन्होंने कभी ऐसी कोशिश भी नहीं अपने सपनों में नहीं की होगी। पर, जंगल में अपने बच्चों की सलामती के लिए जानवर भी क्या नहीं करते हैं?
अक्सर, मेरे इहलोक के अनुसार ‘अर्थ’ और उसका ‘शस्त्र’ जीविकोपार्जन पर ही आकर रुक जाता है। अर्थोपार्जन के लिए आत्मनिर्भता अनिवार्य होती है। आत्मा ही तो चेतना को अर्थोपार्जन के लिए प्रेरित कर सकती है। आत्मा की इस पुकार का उतार जीवन हर काल और स्थान पर देता ही आया है। हर रूप में वह ज़रूरी ही था, और ज़रूरी ही रहेगा। पर, यहाँ तो प्रेरणा भी लोकतंत्र की दहसत से घबराये-घबराये मुँह छुपाये यहाँ-वहाँ भटक रही है। ऐसे में कोई ख़ुद को अभिव्यक्त भी कैसे करेगा? जब आभासी अभिव्यक्ति और काल्पनिक स्वतंत्रता का प्रचार-प्रसार यह लोकतंत्र ही करता रहेगा। कैसे मेरा इहलोक अपने लिए एक सपना बन पाने की कोशिश भी करेगा? जब यह लोकतंत्र ही मुझसे चमत्कार की अपेक्षा पाले रहेगा।
हर कोई जादू या चमत्कार नहीं कर सकता है। ना जाने एक ही ईश्वर ने ऐसा पक्षपात क्यों किया कि हर प्राणी को समानता के अधिकार से वंचित कर दिया? चलो, गलती से उन्होंने अगर ऐसा कर भी दिया, तो हमने उसे ईश्वर क्यों मान लिया? मान भी लिया, तो उसे एक क्यों नहीं जाना? अगर जान ही लिया है, तो उसका नाम क्या है? बताओ!
यहाँ कोई कुत्ता है, तो कोई बिल्ली, तो कोई गटर में पिल्लू सा अपना जीवन गुज़ार रहा है। बिना व्यक्तित्व के मनुष्य और वस्तु में अंतर ही क्या बच जाता है?
मेरे इहलोक में तो हर कोई अपने सपनों का शहंशाह है, जिसे जीविकोपार्जन के लिए कुबेर का ख़ज़ाना चाहिये। हर कोई कल्पतरु की कामना लिए प्रार्थना किए जा रहा है। ऐसी प्रार्थनाओं का किसी धर्म से क्या लेना-देना है? क्या धर्म का काम बच्चे पैदा करना, या उनका लिंग निर्धारित करना है? कल ही लोकतंत्र ने मेरे इहलोक में रहने वाले एक पिता की यह कहानी सुनायी। जिसे पढ़कर मुझे लगा कि काश, काश यह बस किसी की कल्पना ही होती। एक पिता ने बेटा पैदा करने के लिए अपनी दो बेटियों का दस साल तक बलात्कार किया। यह उसी राज्य की खबर है, जिस राज्य का मैं निवासी हूँ। जहां मेरी शिक्षा-दीक्षा हुई है। जहां मैं अपनी बेटी भी पालता हूँ। मैं ऐसी कल्पना कर भी डर जाता हूँ। मेरा इहलोक ऐसे सच को भी पचा जाता है। डकार तक नहीं लेता!
अपनी आदर्श अवधारणाओं को हर कोई अपनी आँखों से देखना चाहता है। इसलिए, लोकतंत्र वही दिखाने की कोशिश करता है, जो लोक देखना चाहता है। पर चाहत का कल्पनाओं से वास्ता है, चाहकर भी हम कब अपनी महबूबा के दमन पर चाँद-तारे सजा पाये हैं? बहुत हुआ, तो औकतानुसार कुछ चमकीले पत्थरों का हार बाज़ार से ख़रीदकर ले आते हैं। लोकतंत्र तो बस वह आईना है, जिसमें हम अपनी सामाजिक छवि को निहारकर अपनी सुंदरता का अनुमान लगा पाते हैं। हम जैसे होंगे लोकतंत्र हमें वैसा ही दिन दिखलायेगा। कुछ लोगों के अच्छे दिन तो सच में चालू हैं। किसके? इसी का अनुमान लगाना में ही ही तो मेरा इहलोक व्यस्त है। अनुमान के इस ज्ञान का व्यापार ही तो शिक्षा का रोज़गार बन चुका है। पर, पाठशाला में ही हर ज्ञान कहाँ मिलता है?
कुछ ज्ञान हमें जीवन की मधुशाला से भी तो प्राप्त हो पता है। कितनी मज़ेदार बात है कि बच्चन साहब की मधुशाला से मधु हटाकर पाठ ले आने से भी उसके अर्थ में कोई ख़ास अंतर नहीं आ जाता है। अपने इहलोकतंत्र में मैंने पहले भी कहीं यह उदाहरण दिया था। मधुशाला की कुछ रुबाइयों को यहाँ शिक्षा के वास्ते थोड़ा और बिगाड़ लेते हैं।
भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला,
कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला,
कभी न कण-भर खाली होगा लाख पिएँ, दो लाख पिएँ!
पाठकगण हैं पढ़नेवाले, पुस्तक मेरी पाठशाला!
मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला,
प्रियतम, अपने ही हाथों से आज पढ़ाऊँगा प्याला,
पहले भोग लगा लूँ तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा,
सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी पाठशाला!
अगर ऐसी पाठशाला शायद बच्चन साहब को भी मिली होती, तो उन्होंने भी संभवतः अपनी रचना का नाम ‘पाठशाला’ रखने पर विचार किया होता। पर उनके हाथ में जो कलम थी, वह भी हाल ही उगल रही थी। अपने इहलोक में उन्हें भी जीवन मधुशाला में ही नज़र आयी। आज भी हमें पाठशालाओं में अज्ञानता का ही पाठ पढ़ाया जा रहा है। हमारी अभिव्यक्ति से ज़्यादा जहां हमारी स्मरणशक्ति की परीक्षा तंत्र ही ले रहा है, और परिणाम भी वही देता आया है। ऐसे ही चलता रहा तो तंत्र ही प्रमाण देता जाएगा। ना जाने, मेरा इहलोक अपने और बच्चों के लिए जीवन से भरी पाठशाला की माँग कब लोकतंत्र से कर पाएगा?
