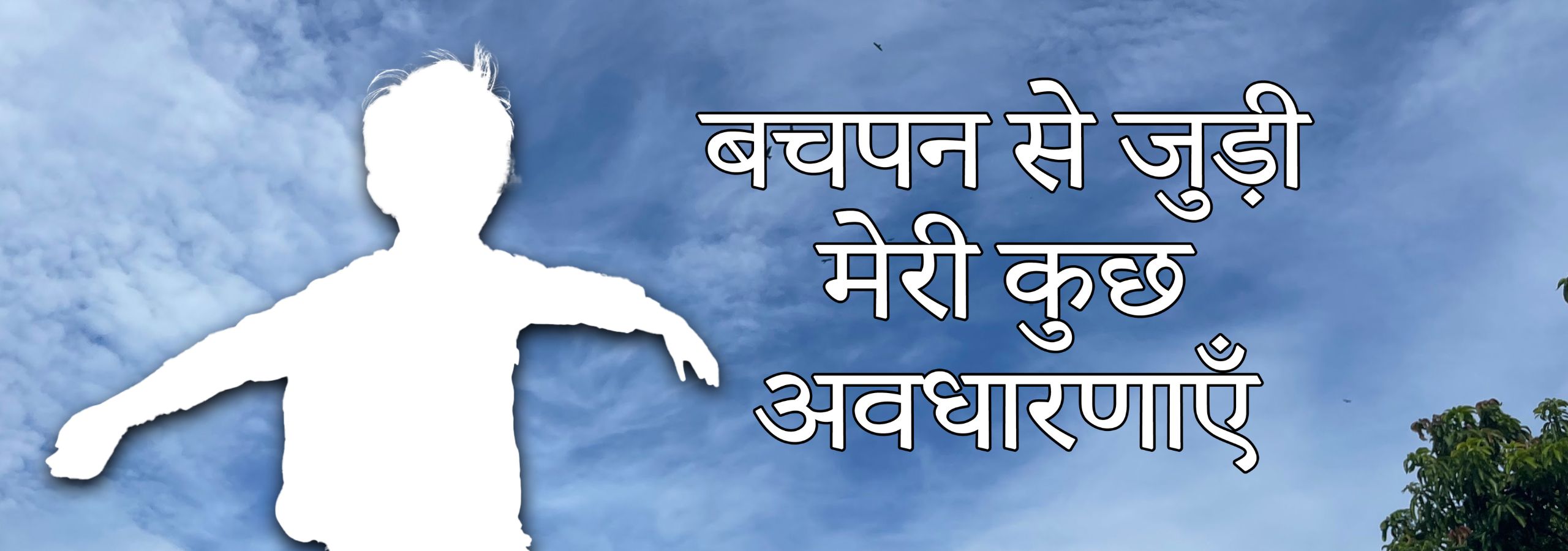वापस लौटकर अगर हम अपना बचपन बदल पाते, तो क्या बात होती?
सबसे अजीब बात है कि सिर्फ़ अकेला मैं ही नहीं हूँ, जो काल-यात्रा कर अपना अतीत बदल देने चाहता है। ख़ासकर, हर किसी को अपने-अपने बचपन से कई शिकायतें होती हैं। हर किसी का बस चले तो वह अपने माता-पिता को भी बदल डाले। अब चाहे उसका बाप कुबेर और माता सरस्वती ही क्यों ना हो? ऐसी लालसाओं की शिकार प्रायः हर चेतना है।
क्या अपने-अपने अतीत को स्वीकार कर पाना हमारे लिए इतना कठिन है?
ज़ाहिर है, कठिन तो होगा ही। वरना, हर कोई संतुष्ट ना हो जाता। मेरे अनुसार संतोष के बिना नैतिकता के हर गुण गौण हो जाते हैं। बिना संतोष के अहिंसा कैसे संभव है? नीतिशास्त्र में अहिंसा सिर्फ़ शारीरिक या भौतिक नहीं है। नीति-निर्धारण के लिए अहिंसा के मानसिक और आध्यात्मिक पहलू भी महत्वपूर्ण हैं। अतृप्ति चेतना अपने-आप में हिंसात्मक ही हो सकती है। एक संतुष्ट व्यक्ति हिंसा के बारे में सोचेगा भी क्यों? जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं, तो किस बात के लिए वह संघर्ष करेगा। जीवन के सागर में संघर्ष के मंथन से ही अहिंसा का अमृत निकलता है।
परिस्थिति-जन्य असंतोष ही तो हमें सत्य के ज्ञान से वंचित कर देता है। सत्य अखंडित है, और संतोष भी। आपने कभी किसी संत को चोरी करते देख है? अगर देखा भी है, फिर भी आप उसे संत मानते हैं। तब तो आपको अपनी विद्वता पर अहंकार भी होता होगा। क्या किसी संत का जीवन भोग-विलास से लिप्त होना चाहिए? अगर संत ही असंतुष्ट है, चोरी कर अपना घर भरता है। तो, वैसे समाज को नीतिशास्त्र की ज़रूरत ही क्या है? प्रेम और करुणा की अपेक्षा भी फिर किसी चेतना में कहाँ संभव है? संतोष को भय कैसा?
संतोष अगर होता, तो भ्रष्टाचार कैसे होते?
मतलब, तार्किक स्तर पर यह मान लेना कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर संतोष ज़रूरी है, कहीं से ग़लत नहीं होगा। तो सवाल यह उठता है कि यह संतोष कहाँ और कैसे मिलेगा? व्यक्ति कब और कैसे संतुष्ट हो सकता है?
भूख से बिलखता नवजात शिशु असंतुष्ट है। परमहंस तुल्य बाल काल भी अतृप्त है। उसे कभी खिलौना चाहिए, तो कभी चिप्स-कुरकुरे, तो कभी चाय, कोल्ड-ड्रिंक की फ़रमाइश करता बचपन, अपनी ही महत्वाकांक्षाओं का ग़ुलाम है। शिक्षा और समाज उसकी महत्वाकांक्षाओं को भड़काता ही जाता है। औक़ात के ऊपर की आमदनी किसे अच्छी नहीं लगती? जवानी से लेकर बुढ़ापा तक इस अनुरक्ति, अभक्ति, अश्रद्धा, असन्तुष्टि का शिकार है। ऐसे ही भागते-दौड़ते जीवन की कल्पना हम अपने बच्चों की दिखा-सीखा रहे हैं। उसके बाद यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अभय हो, धार्मिक हो, सर्वगुण-संपन्न हो!
धर्म की रक्षा कैसे होती है? क्या बस दूसरे धर्म वालों को मार-काट देने से हम धार्मिक हो जाते हैं? यह मंदिर वहीं बनेगा, नहीं वहाँ मस्जिद बनेगा, क्या ऐसे वादे-दावे करने से समाज और राजनीति नैतिक बनती जा रही है? यह लोकतंत्र किस अज्ञानता का शिकार हुए जा रहा है?
बचपन में जब से मैंने होश सम्भाला है, कभी-कहीं चैन और सुकून से मुलाक़ात नहीं हुई है। संतोष भला कहाँ मिलता?
हर दिन स्कूल जाना भला क्यों ज़रूरी है? क्या हम अपनी मर्ज़ी से स्कूल तक नहीं जा सकते हैं?
पाँच-दस साल के छोटे-छोटे, मासूम बच्चे अपने माता-पिता के इस अत्याचार के शिकार हैं। क्यों यह अत्याचार खुलेआम चालू है?
क्योंकि, हम एक असंतुष्ट माता या पिता हैं। यह असंतोष क्यों है?
क्योंकि, हम सब डरे हुए हैं। हम इतना क्यों डरे हुए हैं?
यह एक काल्पनिक डर है। हर चेतना कल्पना करने के लिए स्वतंत्र है। किसी को डर की कल्पना करने से भी भला कौन रोक सकता है?
पहली या दूसरी कक्षा में पचास-साठ बच्चों के बीच मुझे कक्षा में ग्यारहवाँ स्थान मिला था। फिर भी मेरी माँ संतुष्ट नहीं थी। मैंने भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ अगरबत्ती-मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई शुरू की, अगली परीक्षा में मुझे चौथा स्थान मिला। माँ खुश हुई, पर संतुष्ट तब भी नहीं थी। अब और मेहनत करना, मेरी औक़ात से बाहर था। थक-हारकर मैंने मेहनत करना ही छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि मैं तीसरी कक्षा की इकाई जाँच परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया। विषय शायद अंग्रेज़ी था। माँ ने मेरे रिपोर्ट कार्ड को बहुत सम्भालकर रखा था। मुझे वह कई बार दिखाती थी। मेरी ऐकडेमिक प्रगति पर उनकी पैनी नज़र थी। मैं हतास हो गया। फेल होकर जब घर आया तो पिताजी मुझे गले लगाकर रोये। वे सब कितने ग़रीब और असंतुष्ट नज़र आते थे। आज भी वे असंतुष्ट ही हैं — मुझसे भी, ख़ुद से भी।
यह मनोदशा अगर सिर्फ़ मेरे इहलोक की होती, तो मैं शांत बैठ जाता। यही हड़कंप हर इहलोक में मचा हुआ है।
पढ़ाई के बिना कमाई पर ख़तरा, और कमाई के बिना लुग़ाई का ख़तरा!
मेरे पड़ोस का हर इहलोक इसी असंतोष से ग्रस्त है। अपनी चार साल की बेटी से आज मैंने पूछा - “स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है?”
आज सवेरे-सवेरे ही उठकर उसने घर पर स्कूल ना जाने की कवायत शुरू कर दी थी। मुझे मेरा बचपन नज़र आ रहा था। माँ ख़ाना बना रही है, टिफ़िन पैक कर रही है। पिताजी मेरा जूता पॉलिश कर रहे हैं। बस आने वाली है। जल्दी से बस स्टॉप पहुँचना है। स्कूल जाना है। स्कूल में ना जाने दिन-भर क्या चलता रहता था? कभी वहाँ शिक्षक चिल्ला रहे हैं। कभी यहाँ कोई हमें डाँट-फटकार रहा है। आतंक का साया स्कूल पर मंडराता ही रहता था। टिफ़िन में भोजन तक नसीब नहीं होता था। कभी चील झपट्टा मार जाती थी, तो कभी भूखे कुत्ते को हम अपनी रोटियाँ खिला देते थे, क्योंकि उस बासी रोटी को खाने लायक़ हमें भूख नहीं लगी होती थी। माँ को भूखे और भुक्खड़ दोनों तरह के बच्चे बिलकुल अच्छे नहीं लगते हैं। माँ को लगता है कि उनकी संतान बिलकुल उनके नियम-क़ानूनों पर चले। पिताजी का भी यही सपना है। बच्चा इस पारिवारिक व्यवस्था में ख़ुद के लिए कल्पना करने को भी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए, बाक़ी परिवार, पड़ोस और समाज भी अपनी-अपनी कल्पनाओं का बोझ हमारे ऊपर लादता जाता है।
उसी बोझ तले आज मैं अपनी बेटी को रोते-बिलखते देख रहा था। मेरे सवाल का उत्तर उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सोचकर उसने कहा - “कल से नहीं रोऊँगी, पापा! अभी फ़ोन देखने दे दो!”
उसके दादाजी पिछले कुछ दिनों से चिंतित थे कि उनकी पोती स्कूल क्यों नहीं जाती है?
उन्होंने मुझसे पूछा था - “आर्ची को स्कूल भेजना चाहिए। जब-तक उड़ने के काबिल न हो जाए,तब तक पढ़ाना चाहिए। संसार जो सामने है, उसकी अच्छाई बुराई से परिचय होना चाहिए।”
बदले में मैंने भी उनसे पूछा था - “वह जाना ही नहीं चाहती है। मैं क्या कर सकता हूँ। बोलती है मम्मी के साथ ही जाएगी। वैसे भी पढ़-लिखकर किसका भला हुआ है?”
पिताजी का गंभीर जवाब आया - “भला-बुरा का अपना परिपेक्ष्य है। कम से कम पढ़ने लिखने आ जाय। अगर उसे इंगेजमेंट नहीं मिलेगा, तो मोबाइल आदि में लगी रहेगी। क्या यह सही होगा?”
“बिलकुल इसमें ग़लत ही क्या है?”
“मुझे लगता है कि स्कूल जाना चाहिए। बुनियादी समझ के बाद उसे जो भी रास्ता अपनाना होगा, अपनायेगी।”
“पढ़ लिखकर भी इंसान नौकरी ही करता है। अनपढ़ आदमी भी किसी का नौकर ही बनता है। बुनियादी समझ तो दोनों में होती है।”
“ठीक है।”
“ठीक है।”
बात ख़त्म हो गई। पिताजी मेरी अवधारणाओं से पूर्णतः असहमत हैं। मैं ख़ुद अपनी अवधारणाओं से असहमत हूँ। मेरे हिसाब से भी बच्चों को स्कूल जाना ही चाहिये। पढ़ना ही चाहिए। कुछ रचना-गढ़ना सीखना ही चाहिए। ज्ञान को हासिल कर ख़ुद के लिए एक बेहतरीन कल्पना को रचने का उसे मौलिक अधिकार है। देश का संविधान उसे यह अधिकार देता है। पर, अफ़सोस! इस देश की दस प्रतिशत आबादी ने भी संविधान पढ़ा ही नहीं है। उसमें भी सौ में किसी एक को कुछ समझ में आता होगा। मैंने तो कई बार पढ़ी है। मुझे ही आज तक ठीक से उसकी हर बात समझ कहाँ आती है?
पर, मेरे घर में बचपन से संविधान की एक प्रति बड़े किराने से रखी रहती थी। आज तो उसके ऊपर आधारित दर्जन भर किताबें तो मैंने जमा कर रखी है। पिताजी के पास तो और भी ना जाने कितनी होंगी? पिताजी ने रामायण-महाभारत, क़ुरान-शरीफ, बाइबिल आदि के ऊपर संविधान को सजा रखा था। मैंने भी पिताजी से सवाल किए होंगे, उन्होंने स्वेक्षा से भी मुझे इन किताबों और उनके महत्व के बारे में समझाया होगा। जो भी था, बचपन से इनके बारे में मेरे अंदर अवधारणाएँ बनती-बिगड़ती आयी हैं, जिसकी गवाह मेरी स्मृति और चेतना है।
मेरी आत्म-अवधारणाओं का अपना ही एक इतिहास है। सब कुछ लिख पाने के लिए किसी भाषा में शब्द ही प्रयाप्त कहाँ हैं?
भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपनी मातृभाषा से बेहतर कोई भाषा नहीं हो सकती है। मेरी मातृभाषा हिन्दी है। इसलिए, यहाँ मैं ख़ुद को स्वतंत्र पाता हूँ। पुस्तकालय के बीच पला-बढ़ा बचपन साहित्यिक तो होगा ही। मेरी इस अवधारणा को समाज ने भी प्रमाणित किया है। जब मेरे हिन्दी वाले मास्टरजी ने मुझसे कहा था - “हिन्दी तो तुम्हारे खून में बस्ती है।”
मैं लेखक बनना चाहता था। तब से जब से मैंने हैरी-पॉटर को पढ़ा था। इन घटनाओं का ज़िक्र मैं शायद पहले भी अपने इहलोकतंत्र में कर चुका हूँ। ख़ैर, अगले ही दिन हमारे संत जोसेफ विद्यालय में बलात्कार वाली वारदात मेरे सामने आ गई। पिताजी के साथ मेरा ह्वाट्सऐप संवाद कुछ इस प्रकार था —
मैं - “फ़ेसबुक पर एक दो ऐसे पोस्ट देखकर मैंने अभी गूगल पर जानने का प्रयास किया कि आख़िर माजरा क्या है?
देखकर चेतना दहल गई।
उसके बाद जब मैंने इन पोस्ट और सामाजिक प्रतिक्रिया का जायज़ा लिया, तो इस लोक से ही भरोसा उठ गया।
ये अभी भी आवाज़ उठाने से डरते हैं?
दबी हुई अवाज में खुसुरपुसुर चल रही है। स्कूल में अभी भी बच्चों को भेजा जा रहा है? क्या कोई माता-पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करता?
उस स्कूल ने पहले ही मेरे बचपन का नाजायज़ शोषण किया। अपनी बच्ची के सामूहिक बलात्कार हो जाने का मैं इंतज़ार करूँ?
किस मुँह से आप बोलते हैं कि आर्ची स्कूल क्यों नहीं जाती है?
किस मुँह से उसे मैं स्कूल भेजूँ?
जब मैं वहाँ पढ़ा करता था, योग वाले मास्टरजी लड़कियों के स्कर्ट के अंदर हाथ डालकर यह देखते थे कि किसने चड्डी पहनी है? किसने नहीं?
कई बार शिकायत के बाद उन्हें हटाया गया था। क्या आप शर्मिंदा नहीं हैं कि आप लोगों ने मुझे वहाँ पढ़ाया है?
मैं तो बहुत पहले ही शर्मिंदा था। अब तो शर्म करने लायक़ भी हालात नहीं हैं। जिस देश में शिक्षकों से बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, वह देश जीने लायक़ भी है क्या?
यहाँ लाखों रुपये लगते हैं, बीएड की डिग्री हासिल करने में। पान की टपरी की तरह खुले हैं ये प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान, जहां हर चीज बिकाऊ है। आपने भी तो अनिशा के लिये पैसे भरे थे। आप लोकपाल हैं, इन्हें तत्कालीन बंद करवाने का आवेदन तो लिख ही सकते हैं। शिक्षा की इतनी भी ज़िम्मेदारी सरकार नहीं लेगी, तो शराबबंदी से बड़ा जग कल्याण हो जायेगा!
अपने स्कूल वाले ह्वाट्सऐप ग्रुप की कहानी भी मैंने आपको सुनायी है। क्या अब कोई आंदोलन पर्याप्त है?
मेरी समझ से क्रांति ही इकलौता रास्ता हमारे सामने है। एक पीढ़ी को बग़ावत करनी पड़ेगी। तभी वो प्रलय आएगा, जहां से जीवन फिर खिलखिलायेगा।
मम्मी के स्कूल में मेरी मेहनत के अस्सी हज़ार का चेक उनके हाथों भिजवा कर उनसे वापस भी मँगवा लिया। उस स्कूल ख़िदमत में खर्च होती अपनी माँ के इस जीवन को मैं कैसे स्वीकार करूँ? जहां ना ढंग की कोई प्रयोगशाला है, ना ही पुस्तकालय। मैंने उस स्कूल की व्यवस्था को अंदर से देखा है। गिनी चुनी किताबें भी वहाँ धूल फाँक रही थी। उस स्कूल में इतना अर्थ ही कभी मुझे नज़र नहीं आया था कि मेरी मेहनत की वह कदर कर पाता।
इस लोकतंत्र को नया तंत्र नहीं, पहले इसे एक नया लोक चाहिए।
यहाँ तो दशा यह है कि लोक उस स्कूल का नाम लेने से भी डर रहे हैं।
”
पिताजी का कोई जवाब नहीं आया। मेरी पत्नी की तबियत पिछले कुछ दिनों से ख़राब थी। उसका गर्भपात करवाना पड़ा था। तबसे आर्ची, हमारी बिटिया स्कूल नहीं गई थी। कहती थी, माँ के ठीक होने के बाद ही जायेगी। घर की देख-भाल करने उसकी मौसी और बुआ भी हमारे घर आयी हुई थी। उसके पास घर पर ही खेलने की क्या कमी थी? जो मैं उसे प्ले-स्कूल भेजूँ, उस पर भी जब ना प्राइवेट, ना ही सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर अपने बच्चों को भेजने लायक़ है। प्ले स्कूल में आधे टाइम तो भजन-कीर्तन चलता है। बेकार ही सुबह-सुबह भगवान को भी अपने स्वार्थ की लिए हम जगा देते हैं। आराम से सोना कौन सा पाप है?
“स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है?”
इसका जवाब ना मेरी बेटी के पास है, ना ही उसके बाप-दादा के पास।
कई बार सवाल बदलने के बाद, जब यह सवाल उसके सामने आया कि बताओ - “स्कूल में क्या होता है?”
थोड़ा माथा खुजाकर उसने चीखकर कहा - “पढ़ाई!”
उसे यक़ीन था, उसका यह जवाब सही था। पर, वह इस बात को भूल गई थी कि वह अभी तक एक प्ले-स्कूल ही जाती है। उसका सही जवाब सुनकर हम सब भी अपना सवाल भूल गये। बात ही पलट गई। मेरी पत्नी सुबह-सुबह अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से हुई मुलाक़ात के बारे में सुनाने लगी। उसने बताया - “पता है! आज सवेरे-सवेरे बीएड कॉलेज वाले प्रधानाचार्य हमारे घर आये थे। एक चौकोर सा कला रंग का झोला अपनी तोंद पर टिकाये, पूछ रहे थे - ‘सर हैं क्या?’
उन्हें देखकर मुझे लगा कि दिखते तो ये हमारे प्राचार्य जैसे हैं, पर इन्होंने मुनिमजी का हुलिया क्यों बना रखा है?”
इतना सुनकर ही मेरी हंसी छूट गई। आगे की मुक़ालत का हवाला वह देती गई और मेरे ठहाके गूंजते गये।
आगे उसने कहा - “पापा घर पर थे नहीं, मैंने उन्हें बताया, फिर उनके सवालिये चेहरे को देखकर मैंने उन्हें झुककर सलाम किया और बैठने के लिए कहा। ऐसा लगा रहा था कि वे मुझसे पूछ रहे हों कि पहचाना नहीं, बेटी! मैं तेरे कॉलेज का प्रधानाचार्य।
उनका चेहरा देखकर मैं अब पहचान गई थी। वही टिक्की और तिलकधारी प्रिंसिपल जो हर बात के पैसे माँगता था। ना जाने आज क्या माँगने यहाँ पहुँच गया है?
पैर छूने का वक़्त गुजर चुका था। वैसे भी झुकने लायक़ मेरी हालत थी नहीं। मैंने आर्ची को वहाँ बैठाया और अंदर फ़ोन लेने आ गई। वापस पहुँची तो आर्ची फ़ोन छीनकर दादाजी से बात करने लगी उसने बस इतना कहा - ‘दादाजी! आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं नहीं गई।’, और फ़ोन काट दिया। बेचारे प्रधानचार्य महोदय आर्ची का मुँह देखते रह गये।॰॰॰
शायद उन्हें उम्मीद थी कि आर्ची या मैं पापा को फ़ोन पर पूछेंगे कि वे कब तक आयेंगे?
यहाँ आर्ची से फ़ोन ही काट दिया। दुबारा फ़ोन करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। बेचारे प्रधानाचार्य महोदय कब उठकर चले गये, पता ही चला॰॰॰
”
मैंने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया और अपनी बेटी को शबासी दी, कहा - “बिलकुल ठीक किया। हम भी जब इनके दफ़्तर जाते हैं ना, तो ये लोग भी ऐसे ही बतियाते हैं।”
पत्नी से मैंने अपनी आशंका ज़ाहिर कि कहीं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों पर मेरे कहने पर पिताजी ने तंत्र से इनपर किसी कार्यवाही की माँग तो नहीं कर दी है। मैं आशंका ज़ाहिर कर ही रहा था कि पिताजी साक्षात पधार गये, और ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गये।
असंतोष तो हमारा पैदाइशी अवगुण है। संतोष के लिए ही तो हमें शिक्षा, ज्ञान और प्रज्ञा की ज़रूरत पड़ती है। पर यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा है। पूरी की पूरी ज्ञान की गंगा ही उल्टी बह रही है। परिवार, समाज और शिक्षा ही हमें असंतुष्ट रहने का पाठ पढ़ाये जा रहा है। फिर, यही लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है।
जो भी, जैसी भी मेरी अवधारणा इस परिवार और समाज के लिए बनी, वह कहीं से मुझे जीवन के पक्ष में तो नज़र नहीं आती है। निश्चय ही मैं ग़लत हो सकता हूँ। पर उन प्रमाणों का क्या जो मैं देता आया हूँ?
मेरी तो दिली तमन्ना है कि आप मुझे ग़लत साबित कर दें। मेरे इस भ्रम को तोड़ दीजियेगा, तब भी मेरा इहलोक सुधार जाएगा। वरना, इस लोकतंत्र को मेरी कुछ बातों पर गौर तो करना ही पड़ेगा। मेरी किसी भी बात मान लेना भी ज़रूरी नहीं है। पर, सुन लेने में किसी का क्या बिगड़ जाएगा?
सुन तो लीजिये, शायद हम दोनों का इहलोक हक़ीक़त में बेहतर हो जाये!