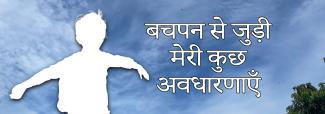एक लोकतांत्रिक अवतार
मेरे अनुमान से इस शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और दार्शनिक दोष है। हमारे इतिहास में आज तक पुनर्जागरण काल नहीं आया, जब जनमानस को अपनी रचना-शक्ति पर आस्था हो। यह आस्था ही थी जिसने साहित्य, कला के रास्ते उद्योग की रचना की। हमारे आदिकाल में ही कहीं स्वर्ण-युग की तलाश में देश और काल की जवानी बर्बाद हुए जा रही है। सृजन की संभावना कुछ युवाओं को दिखती भी हैं। पर, वे छोटी-मोटी उपलब्धि से ही संतुष्ट हो जाते हैं। वे सत्याग्रह नहीं करते। वे अपने सच को ही सत्य मान बैठते हैं। मुझे उनकी दरिदता पर तरस भी आता है। मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता हूँ। हिन्दी विभाग के सृजनशील शिक्षकों की बातों से भी मुझे निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। अनुभव में भी वे दरिद्रता ही तलाशते मिले। मैं भी किसी का अपमान नहीं करना चाहता, शौक़ से गालियाँ देता हूँ, पर किसी की भावना को चोट पहुँचाने की प्रवृति मेरी तो नहीं।