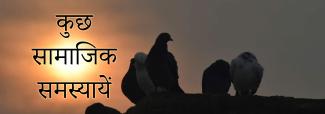लोक-माया-तंत्र-जाल
देश में ना मौजूदा प्रशासन और ना ही वर्तमान राजनीति को लोक या जनता की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर को तो आपकी या मेरी, या हमारे बच्चों की कभी चिंता थी ही नहीं! इसलिए तो तंत्र तानाशाह बन गया है। इनकम टैक्स से लेकर टोल टैक्स तक सीधे जनता के खाते से तंत्र के खाते में पहुँच रहा है। इधर, इहलोक में शायद ही कोई बचा है, जो अपने बच्चे से भी प्यार करता है। फिर भी आपको लगता है कि लोकतंत्र बचा हुआ है, और उसे बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो मेरी तरफ़ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ!