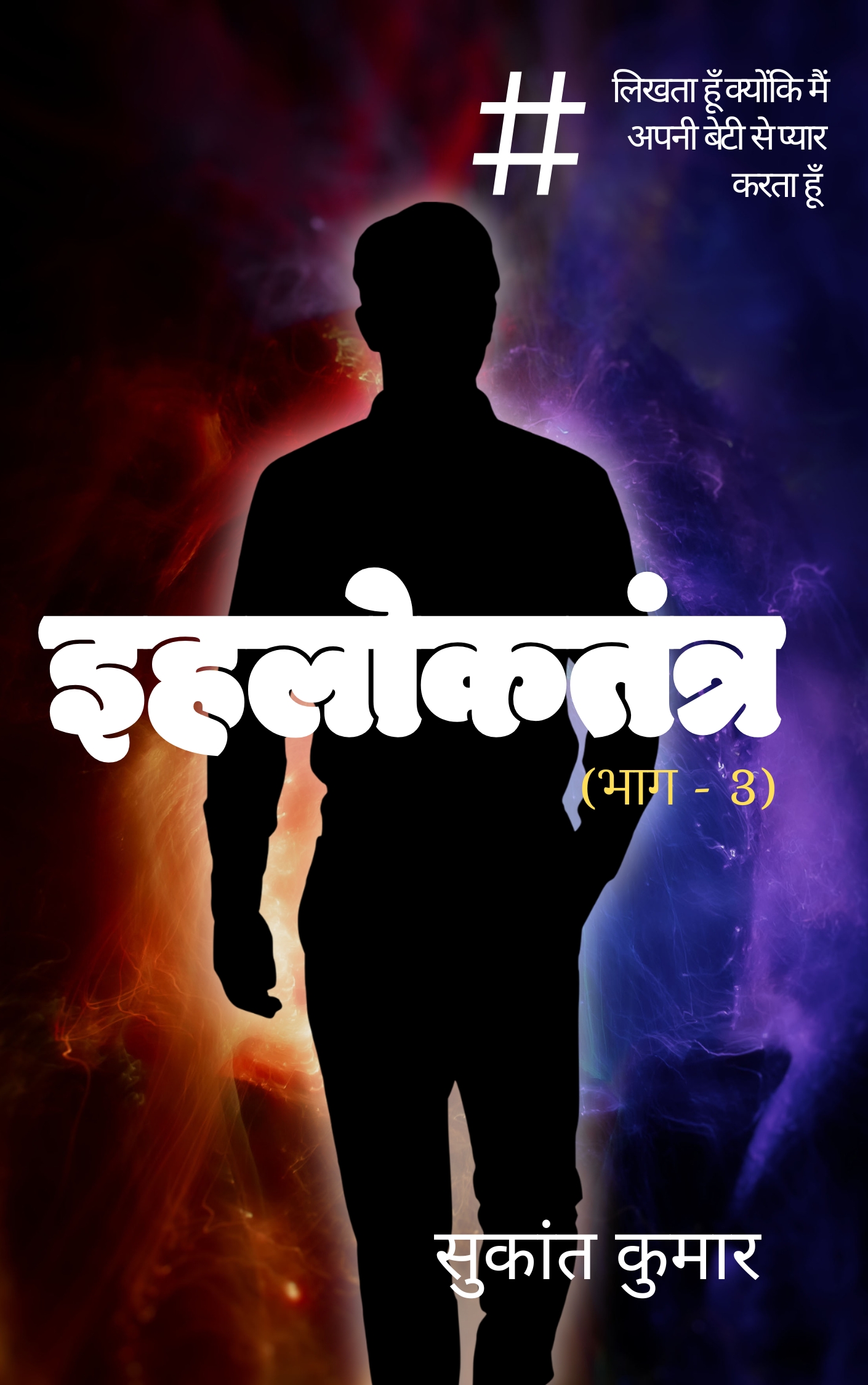 प्रस्तावना
प्रस्तावना
दिनांक: 6 अक्टूबर, 2023
यह कोई साहित्यिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक या किसी अन्य निर्धारित शैली की किताब नहीं है। अतः इसे साहित्य का हिस्सा ही मान लेना उचित होगा। कला या साहित्य की सबसे ख़ास बात होती है कि यहाँ एक रचयिता को प्रमाण देने की कोई मजबूरी नहीं होती है, साथ ही उसे सबूत रचने की स्वतंत्रता भी होती है। साहित्य के पाठकों की आस्था भी यहाँ आज़ाद होती है। पाठक भरोसा करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। विज्ञान के विद्यार्थियों के पास इस स्वतंत्रता का अभाव होता है। उन्हें किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए प्रमाणों को ख़ुद के लिए विधिवत रूप से स्थापित करना पड़ता है। तभी तो विज्ञान की शिक्षा प्रयोग के बिना अधूरी ही रहती है।
अपने व्यक्तिगत शैक्षणिक अनुभवों में मैंने महसूस किया है कि हम प्रयोग करने के लिए भी आज़ाद नहीं हैं। कल्पना करने की अभिन्न चेतना भी ना जाने कहाँ विलीन है? जहां कल्पनाओं पर भी पहरा लगा हो, वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी भी कहाँ संभव जान पड़ती है। मेरी समझ से यह पुस्तक मेरे अस्तित्व की अभिव्यक्ति मात्र है — ख़ुद को अभिव्यक्त कर पाने की जद्दोजहद, मेरी बग़ावत और उसकी कहानी है। यहाँ आपको मेरी अनुभूतियों, अवधारणाओं और कल्पनाओं का विवरण मिलेगा। साथ ही मेरे सामाजिक अनुभवों का ब्योरा भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ मेरे लोकतांत्रिक सुख-दुख की कहानियाँ भी मिलेंगी, जिन्हें मैंने अपने इहलोक में झेला है। यहाँ मैं हूँ। सवाल सिर्फ़ इतना है कि — क्या मैं इतना ज़रूरी हूँ? क्या आपकी अनमोल चेतना में मेरा होना ज़रूरी है? क्या मैं आपके क़ीमती समय के लायक़ हूँ भी या नहीं?
यहाँ मैं अपने अस्तित्व की ज़रूरत और उसकी ज़रूरतों को जानने-समझने का उपाय ढूँढ रहा हूँ। किसी भी रचना को आपके थोड़ा धैर्य की अपेक्षा तो रहती ही है। मैं ख़ुद को बहुत ही चयनात्मक पाठक मानता हूँ। हर किताब मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाती हैं। किसी पुस्तक का औचित्य, परिकल्पना, भूमिका, लेखक-परिचय, आदि-आदि के आधार पर मैं उस किताब के बारे में ख़ुद के लिए एक अवधारणा निर्धारित करता हूँ। थोड़ा शोध करने के बाद ही मैं किसी किताब को पढ़ने या ना पढ़ने का फ़ैसला करता आया हूँ। आज तक किसी भी शैक्षणिक कोर्स में यह बुनियादी स्वतंत्रता मुझे नदारद ही मिली है। हर किताब को समझ लेना मैं अपने लिए ज़रूरी भी नहीं समझता हूँ। किसी भी व्यक्ति के लिए दुनिया की हर किताब को पढ़ लेना संभव भी नहीं है। मेरा अध्ययन विस्तृत होते हुए भी बड़ा सीमित है। कभी-कभी तो लगता है कि किसी कुएं के अंदर बैठा टर-टर करता मेंढक हूँ, मैं।
ख़ैर, अब एक लेखक के रूप में मैं अपने लिए एक सामाजिक स्थान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं अपने औचित्य को अभिव्यक्त कर देना ज़रूरी समझता हूँ।
समस्या और समाधान के बीच ही ज्ञान झूलता रहता है। कुछ समाधान तो समस्या को नकार देने से ही मिल जाते हैं। हर व्यक्ति और समाज के सामने अलग-अलग और अनेक समस्याएँ हैं। मेरी वर्तमान मुख्य समस्या देश का मौजूदा लोकतंत्र है। मेरे अनुमान से इस लोकतंत्र की जड़ें शिक्षा व्यवस्था की दरिद्रता से कुपोषित हो गई हैं। इस रचना के केंद्र में लोक भी है और तंत्र भी है। समाधान भी अक्सर वहीं मिलता है, जहां समस्या होती है। मेरे अनुमान से हमारी लोकतांत्रिक समस्यायें सिर्फ़ तंत्र में ही निहित नहीं है। लोकतंत्र की अवधारणा ही लोक पर आधारित है। तंत्र की ज़िम्मेदारी तो संचालन मात्र की है। लोकतंत्र के केंद्र में तंत्र नहीं लोक है।
पारिभाषिक स्तर पर भी देखें तो लोकतंत्र को सुचारू ढंग से चलाने की ज़िम्मेदारी तंत्र की कम और लोक की ज़्यादा है। अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए मैंने लोक और तंत्र को अलग कर लिया है। अपनी कल्पनाओं को शब्द देने के लिए मैंने अपना इहलोक और उसके तंत्र को रचने का बीड़ा उठाया है। मेरे अनुमान से बुनियादी ज़रूरतों और ज़िम्मेदारियों के ज्ञान की कमी में ही तो लोक की अज्ञानता विद्यमान है। ज्ञान का अभाव ही तो अज्ञानता होती है। अभाव और आपूर्ति पर ही तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था आश्रित है। समाज ने अपनी सुविधा के लिए शिक्षा को व्यापार में बदल लिया है। अभाव ही तो व्यापार का आधार बनता है। पर, व्यापारिक नैतिकता या ‘Business Ethics’ भी तो कोई चीज होती है। कॉर्पोरेट संस्कृति का जमाना है। किन चीजों का व्यापार प्रतिबंधित होगा, या लोकहित में किन उत्पादों का आयात-निर्यात होगा, इसका निर्धारण करना ही तो राजनीति की ज़िम्मेदारी होती है। पहले, राजा-महाराजा यह कष्ट उठाते थे, अब यह लोकतंत्र का बोझ है। मेरी समझ से अर्थशास्त्र का दायरा वाणिज्य-शास्त्र से विस्तृत होता है। यहाँ ‘अर्थ’ का अर्थ सिर्फ़ मूल्य नहीं होता है, ज़रूरतें भी यहाँ मूल्यवान होती हैं। शिक्षा को रोज़गार से जोड़ने में मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। पर, उस शिक्षा का क्या फ़ायदा जो हमें नौकर बनाने पर उतारू है?
यहाँ मैं ज्ञान को वर्तमान लोकतंत्र के लिए समझने-समझाने का प्रयास ही तो कर रहा हूँ। इस रचना के हर पाठक को मुझसे सहमत-असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता है। पर, कोई तथ्यों से कैसे असहमत हो सकता है? सरकारी आँकड़ों के अनुसार हर दिन इस देश के ४०-५० छात्र ख़ुदख़ुशी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (अंग्रेजी: National Crime Records Bureau, एन सी आर बी) के अनुसार ८०-१०० बलात्कार के केस हर रोज़ दर्ज हो रहे हैं। हमारे लोकतंत्र की यह दुर्दशा ही मेरी जिज्ञासा का केंद्र बिंदु है। इसलिए भी मेरी समझ से आपको मुझे अपनी बात कहने का एक मौक़ा दे देना चाहिए।
यहाँ अपने अतीत को मैंने प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने की चेष्टा भी की है। ग़लतियों की अन्नत संभावनायें मेरे सामने है। सही होने का एक मात्र रास्ता अभिव्यक्ति ही तो है। ग़लतियों का ज्ञान ही तो तो उसकी अज्ञानता को दूर करने में सक्षम है। मेरे अतीत को किसी नैतिक निर्धारण की दरकार नहीं है। पर, मेरे अनुमानों का सही या ग़लत होना आप पर भी निर्भर करता है। इसका निर्धारण मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपने अनुमान के लिए तर्क ही दे सकता हूँ, और मेरी जानकारी में तर्कों में कोई ज्ञान मौजूद नहीं है। मैं कहीं कभी यह नहीं दावा कर सकता हूँ कि मैं ही सही हूँ। ऐसा कर लेने मात्र से ही मुझे अपनी गलती पर गलनी होने लगती है। मेरे अनुसार भी आप ही सही हैं। क्योंकि, मेरा सही या ग़लत होना ज़रूरी भी नहीं है, बस मैं ज़रूरी हूँ। मेरी अभिव्यक्ति ज़रूरी है। यह ‘मैं’ कोई लेखक नहीं है, यहाँ तो मैं भी एक पाठक ही हूँ। मैं ख़ुद को पढ़ रहा हूँ। मेरी समझ से शिक्षा और समाज का बस इतना ही तो दायित्व है कि वह हमें ख़ुद को पढ़ना और समझना सीखा दे। उसके बाद तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। सब कुछ समझ सकते हैं। अच्छा भी, बुरा भी। दोनों की ज़रूरत और उसकी समग्रता को समझना ही तो ज़रूरी है।
ख़ुद के साथ, यहाँ मैं अपने इहलोक की ज़रूरत को भी समझने-समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ। मेरे अनुमान मेरा इहलोक कई ऐसी अवधारणाओं, भावनाओं और संवेदनाओं को ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी मान बैठा है, जो जीवन के पक्ष में अब नहीं रह गई हैं। काल और स्थान के हिसाब से व्यक्ति और समाज की ज़रूरतें बदलती रहती हैं। नैतिकता भी गतिमान होती है। अगर कुछ शाश्वत है, तो वह जीवन ही तो है। अनुभवों में मैंने अपने लोकतंत्र को ही जीवन के विपक्ष में खड़ा पाया है। जिस लोकतंत्र की बुनियाद ही डर के दम पर क़ायम हो, वह भला जीवन के पक्ष में कैसे हो सकता है? डर में जीवन होता ही कहाँ है?
मैंने देखा है कि शिक्षा से लेकर स्वस्थ जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी डर के साये में व्यापार का साधन बन बैठी हैं। मैंने तो धर्म को सरेआम नीलाम होते देखा है। राजनीति की दुकानें धर्म के नाम पर पाखंड की कालाबाज़ारी दिन-दहाड़े कर रहा है। मेरी आखों के सामने आज भी मेरा दहसत भरा बचपन है। आज भी मैं अपनी चार-साल की बेटी को स्कूल के नाम से डरा हुआ ही पाता हूँ। तभी तो मैं इतना विचलित हूँ। मेरा विचलित होना भी ज़रूरी है। जो कुछ भी मैंने झेला है, वह भी ज़रूरी था। पर मेरी बेटी भी वही सब झेले यह कहाँ से ज़रूरी है?
मैंने इस शिक्षा-व्यवस्था को में कई उपाधियाँ भी हासिल की हैं। पर, इस शिक्षा-व्यवस्था को मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाया। इसका बहुत छोटा ही हिस्सा मैंने जीवन के पक्ष में पाया है। मेरी कल्पनाओं में एक बेहतर शिक्षा-व्यवस्था संभव है। इसलिए, एक बेहतर लोक और उसके तंत्र की कल्पना करना, मैं अपनी दार्शनिक ज़िम्मेदारी समझता हूँ। कुछ शैक्षणिक प्रमाण भी लेखक होने के मेरे अधिकार को स्थापित करने में आपकी मदद कर सकती है। अपने शैक्षणिक जीवन में मैंने दर्शनशास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होने का प्रमाण मेरे पास मौजूद है। उसके पहले इंजीनियरिंग की एक डिग्री के साथ-साथ मैनेजमेंट की भी एक डिग्री मेरी फ़ाइलों में धूल चाट रही है। क्योंकि, नौकरी के अलावा इनकी कोई ज़रूरत आज तक मुझे नहीं जान पड़ी है।
शिक्षा जगत से मेरा अभिन्न रिश्ता रहा है। मेरे माता-पिता दोनों ही हिन्दी साहित्य को पढ़ते-पढ़ाते एचजी उस गृहस्थी को रचते आये हैं, जहां मैं पला-बढ़ा हूँ। सरकारी और ग़ैर-सरकारी दोनों ही शिक्षा-व्यवस्था को मैंने बड़े क़रीब से देखा है। मेरे बचपन का बड़ा हिस्सा इस शहर के सबसे अच्छे कॉलेज के बीचों-बीच स्थित एक आवास में गुजरा है। आज भी मैं जिस प्रोफेसर कॉलोनी में रहता हूँ, ज़ाहिर है वहाँ शिक्षकों के बीच ही रहता हूँ। अपने इन्हीं शैक्षणिक अनुभवों को यहाँ संकलित करने की कोशिश में मैंने इस साहित्य को रचने का फ़ैसला लिया है।
दर्शनशास्त्र के अध्ययन ने मुझे अनुमान लगा पाने की क्षमता दी है। दर्शन पढ़कर मुझे पता चला कि स्मृतियों में ज्ञान का वास नहीं होता है। ना जाने फिर क्यों पूरी ज़िंदगी मेरे शिक्षकों ने मेरी याददाश्त पर इतना ज़ोर दिया था? अपने अतीत को ज़रूरी मानकर मैं ज्ञान की तलाश में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे दार्शनिक या साहित्यिक सफ़र का ना तो यह पहला पड़ाव है, ना ही यह आख़िरी होगा। यह तो बस एक नयी शुरुआत है। जब तक जीवन है, यह रोमांच चलता ही रहेगा। मंज़िलों के बादल जाने से सफ़र का रोमांच बदलता भी रहेगा। पर, आनंद तो सफ़र में है। आज यह रोमांच मेरे साथ चल रहा है। मेरे बाद भी इस रोमांच के लुफ्त को कोई और उठायेगा, जैसे अभी आप उठा रहे हैं। संभवतः, मैं किसी नये रोमांच कि तैयारी कर रहा होऊँगा। मेरे दुख भी मेरे लिये उतने ही ज़रूरी हैं, जितना सुख की ज़रूरत का मुझे बोध होता है। आनंद को तो मैं हर परिस्थिति में अपने साथ पाता हूँ। इस खंड में मुख्यतः मेरा अतीत संकलित है। जिनके आधार पर मैं आगे ख़ुद के लिए अपने इहलोक और उसके तंत्र की कल्पना को रचने का प्रयास भी करने वाला हूँ। यह एक अंतहीन सफ़र है।
यह कहीं से ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सही हूँ। पर अपने इहलोक में बिना किसी प्रमाण के मैं ख़ुद को ग़लत क्यों मानूँ? अपनी अवधारणाओं के ग़लत होने का प्रमाण भी मैं ही तलाशता हूँ। आप भी मेरी मदद कीजिए। प्रमाणों के आधार पर अपनी अवधारणाओं को मान लेना ही तो ज्ञान है। वरना, सत्य को अखंडित है। सत्य का कोई सटीक विपरीतार्थक शब्द भी कहाँ मिलता है? उसके अभाव को ही हम असत्य मान लेते हैं। असत्य भी उतना ही अखंडित है, जितना की सत्य। दुनिया की विभिन्नता उसके अभाव में ही एकता का बोध कर पाने में सक्षम है। मैं आप में से कुछ के लिये सही भी हो सकता हूँ। कुछ मुझे ग़लत भी मान लेंगे। मुझे दोनों से सहानभूति है। पर, सिर्फ़ मुझे ग़लत मान लेना ही काफ़ी नहीं होगा, मुझे ग़लत साबित करने की थोड़ी ज़िम्मेदारी आपकी भी तो है।
साबित करने के बाद ही ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। न्याय भी तो सबूत और गवाहों पर टीका होता है। अंधा होता है, तभी तो उसे तंत्र की बैसाखी कि ज़रूरत होती है। लोक को न्याय देना तंत्र कि ज़िम्मेदारी है। न्याय कभी व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, तभी तो यह एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है। कुछ भी साबित करने के लिए प्रमाण लगते हैं। उन प्रमाणों को समझने-समझाने के लिए तर्क लगते हैं। प्रमाणों के आदान-प्रदान के लिए जब भी समाज भाषा को माध्यम बनाता है, वहाँ तर्कों का प्रयोग होता है। तर्कों की सत्यता के निर्धारण की ज़िम्मेदारी ही तो तर्कशास्त्र निभाता आया है। वरना, दर्शनशास्त्र तो तर्क को ज्ञान का स्रोत तक नहीं मानता है।
भौतिक सच के लिए प्रमाणों को जब भी साहित्य में दर्ज किया जाता है, वह विज्ञान बन जाता है। मूलतः, ‘तर्क’ — साहित्य है। इस हिसाब से तो किताबों में लिखा विज्ञान भी साहित्य है। किताबों में लिखा विज्ञान उसका इतिहास ही तो है। मेरी समझ से जब तक किसी अवधारणा या सिद्धांत का व्यावहारिक प्रयोग नहीं होता है, तब तक वह विज्ञान कैसे हो सकता है? हर ज्ञान के लिए भौतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वहाँ कल्पनाएँ काम आती हैं। ज्ञान की कई अवधारणाओं के पीछे प्रमाण के रूप में कल्पनाएँ ही तो मौजूद हैं। कुछ चीजों को मान लेना पड़ता है। यह मान लेना ही तो भरोसा है, यही तो आस्था है — जिसके बिना कोई ज्ञान संभव ही नहीं है। भाषा की बुनियाद भी आस्था पर ही टिकी है। गणित भी तो एक भाषा ही है। उसका अपना ही एक व्याकरण है। तर्कशास्त्र का योगदान सिर्फ़ इतना ही है कि वह हमारी आस्था को वह आधार देती है। वरना, तर्कों में कोई ज्ञान कहाँ है? भ्रम, संशय, स्मृति की तरह ही तर्क भी तो ‘अप्रमा’ का पात्र है।
ज्ञान और अज्ञानता को तर्कशास्त्र ही तो जोड़ता है। इहलोक को परलोक से तर्क ही जोड़ते आये हैं, यही तर्कशास्त्र ही तो सूचना क्रांति का अगुवा भी है। कंप्यूटर की बुनियाद साहित्य और दर्शन पर ही तो टिकी है। कंप्यूटर बनाने से पहले किसी ने उसकी कल्पना ही तो की होगी। पुष्पकविमान तो हमारे पास आदिकाल से था। पर, उड़नतश्तरी का आविष्कार महर्षि वाल्मीकि ने तो नहीं किया था। इससे पुष्पकविमान के ज्ञान में कोई कमी तो नहीं आ जाती है।
‘0’ या ‘1’, ‘ग़लत’ या ‘सही’ , ‘बुरा’ या ‘अच्छा’, ‘दुख’ या ‘सुख’, ‘मृत्यु’ या ‘जीवन’, या कोई अन्य विरोधाभाषी तत्व कभी अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता है। इनका अस्तित्व ही सापेक्षता से ग्रस्त है। जहां ‘0’ नहीं है, वहाँ ‘1’ है। जहां ‘ग़लत’ नहीं है, वहाँ ‘सही’ है। जहां ‘बुरा’ नहीं है, वहाँ ‘अच्छा’ है। जहां ‘दुख’ नहीं है, वहाँ ‘सुख’ है। जहां ‘मृत्यु’ नहीं है, वहाँ ‘जीवन’ है। अभाव में ही पूर्णता है। नेती ही ब्रह्म को परिभाषित कर सकती है। इस बात को समझ लेना ही तो आनंद है। अपनी ज़रूरत को जान लेना ही तो प्रयाप्त है। तभी तो कोई संतोष कर सकता है। वरना, पैसे वाला हर धनवान रईस कहाँ होता है?
आप मेरे तर्कों से असहमत हो सकते हैं। मेरे प्रमाणों से कोई कैसे असहमत हो सकता है? कोई मेरे सच से असहमत होकर भी क्या हासिल कर लेगा?
इसलिए, मुझे सही मान लेना आपके लिए बिलकुल ज़रूरी नहीं है। मेरी या अपनी ज़रूरत को समझ लेना ही हम सब के लिये ज़रूरी है। यहाँ तो बस मैं ख़ुद की ज़रूरत को समझने-समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कोशिश हम सबको ईमानदारी से करनी चाहिये। शिक्षा-व्यवस्था की मौजूदा दुर्दशा पर यह मेरी टिपण्णी ही तो है। अपने अनुसार मैं जीवन के पक्ष में लिखता हूँ। आप मेरे पक्ष या विपक्ष में हो सकते हैं। होना ही चाहिए। तभी तो लोकतंत्र चल सकता है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना ही तो राम-राज्य की अवधारणा है। स्वराज ही तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बात भी मैंने पढ़ी है। लोकमान्य तिलक को लोकमान्यता यूँ नहीं प्राप्त है। स्वशासित अराजकता ही लोकतंत्र का मूल मक़सद है। लोकतंत्र इसी की व्यावहारिक दरिद्रता ने ही तो मुझे इस समाज और उसकी नैतिक अवधारणाओं पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया है।
यहाँ मैं उन मजबूरियों को शब्द देने का प्रयास भी करूँगा, साथ ही अपने इहलोक और उसके लिये एक बेहतर तंत्र की कल्पना करने की कोशिश भी करूँगा। मैं अपने प्रमाणों के लिए तर्क भी दूँगा। उन तर्कों में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरी अवधारणाओं और कल्पनाओं पर ध्यान देंगे, मेरे तर्कों को नकार देने में ही बुद्धिमानी है। मेरे तर्क तो माध्यम मात्र हैं। ज़रूरी तो आप हैं। हम सब ज़रूरी हैं। तभी तो हम यहाँ है। हमारी ज़रूरत के ख़त्म होते ही, हमारा अस्तित्व मिट जाता है। मुझे अपने परदादा का नाम तक पता नहीं है। शायद ही आप भी जानते होंगे। पर, 564 ईसा पूर्व पैदा हुए बुद्ध के बारे में संभवतः आप भी कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। उन्होंने अपनी ज़रूरत को समझकर हमें समझाने का प्रयास किया था। वह प्रयास आज भी हमारी चेतना में ज़िंदा है। तभी तो उनका अस्तित्व समय और स्थान से ऊपर है।
यही तो जीवन है। उसकी ज़रूरत है। हमें बस अपनी ज़रूरत को समझना है। शिक्षा का बस इतना ही काम है। समाज का भी तो यही लक्ष्य है। ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए ही तो हम सब रोज़गार की तलाश करते हैं। अफ़सोस, तो मुझे यह देखकर होता है कि पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी लोग भी नौकरी ही कर रहे हैं। रोज़गार के महत्व को वे भी शायद समझ नहीं पाते हैं। हर रोज़ जो काम हमें अर्थ दे सके, वही तो हमारा रोज़गार हो सकता है।
मुझे पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं ईमानदारी को सीखने-सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
मेरा मानना है कि ईमानदारी कोई ऐसी “ज़िम्मेदारी” नहीं है, जो एक बार निभा देने से ख़त्म हो जाती है। एक बार अपनी ईमानदारी साबित करने से हम उम्र भर के लिए ईमानदार नहीं हो जाते हैं। मेरे अनुमान से हर समय और स्थान पर अपने लिए ईमानदार बने रहना ही हमारा एक मात्र धर्म है। बाक़ी सभी धार्मिक पंथों की तरह ही मेरा धर्म भी स्वाभाविक रूप से धर्म-निरपेक्ष है। किसी भी सामाजिक या धार्मिक पंथ के साथ, मैं ख़ुद को जोड़ पाने में असमर्थ पाता हूँ। इस समाज में जीवन के प्रति पसरी हुई उदासीनता और सामूहिक नैतिक पतन को देखते हुए ही मैंने अपनी अवधारणाओं और कल्पनाओं को रचने का प्रयास किया है।
इसलिए, एक लेखक के रूप में मैं आपकी तरफ़ से भी जीवन के पक्ष लिखता हूँ!
#लिखता_हूँ_क्योंकि_मैं_अपनी_बेटी_से_प्यार_करता_हूँ
**एक बेरोज़गार दार्शनिक, **
**जो ख़ुद को ‘सामाजिक वैज्ञानिक' भी मानता है,**